From: Khalid <khalidanisansari@gmail.com>
Date: 2010/12/16
Subject: Pasmanda Rajniti ki Rooprekha
To: Palash Biswas <palashbiswaskl@gmail.com>
पसमांदा राजनीति की रूपरेखा
खालिद अनीस अंसारी
हम सब जानते हैं कि भारतीय समाज मुख्यतः वर्ण/जाति आधारित समाज है. यहाँ का इतिहास रहा है कि ऊंची जातियों नें हमेशा कमज़ोर जातियों को दबाया है और उनका मानसिक तथा शारीरिक शोषण किया है. जाति का 'वर्ग' और 'लिंग' के साथ भी गहरा रिश्ता होता है. यह साफ़ तौर पर कहा जा सकता है कि उच्च-जातियों में अमीर और धनवान व्यक्तियों की संख्या ज्यादा होती है और पिछड़ी और दलित जातियों में गरीबों, दरिद्रों और मेहनतकश तबकों की. इस के अलावा महिलाओं को, कुछ कम कुछ ज़्यादा, सारे समूहों में हाशिये में ही रखा जाता है. इन परिघटनाओं का सीधा संबंध जाति व्यवस्था के अनुक्रमिक असमानता (graded inequality), छुआछूत, सह्जातीय विवाह और पुश्तैनी पेशों से बंधा होना जैसे नियमों से है जिन्हें धर्म की वैधता भी प्राप्त है.
जाति आधारित समाज मुख्यतः सत्ता-केंद्रित समाज है जहाँ पर सारी राजनीति, सांस्कृतिक प्रणाली, धार्मिक व्याख्यायें और आर्थिक संरचना का एक ही मकसद होता है: उच्च जातियों के हितों को साधना और सत्ता पर उनके नियंत्रण को बरकरार रखना. किसी भी प्रकार का एकाधिपत्य (monopoly)—चाहे वह ज्ञान, सत्ता, धर्म या धन-दौलत का हो—न सिर्फ अनैतिक है, बल्कि पूरी तरह से अक्षम (inefficient) भी साबित होता है. जाति व्यवस्था ने हमारे मुल्क की अकसरियत दलित-बहुजन आबादी को सत्ता, ज्ञान और अर्थ से दूर रख कर उनकी सजॆनात्मकता और आत्मविश्वास को रौंदने का काम किया. जिसके फलस्वरूप हम अपने चारों ओर गरीबी के समंदर के बीच समृद्धि के छोटे-छोटे टापू देखते हैं. इसके अलावा हमारी तहज़ीब और संस्कृति बुरी तरह से सड़ और खोखली हो चुकी है. अब ज़रूरत है कि एक प्रगतिशील एवं अंधविश्वास-मुक्त समाज की कल्पना की जाये और सामाजिक सुधार के कार्य को गंभीरता से लिया जाये. इन सब मुद्दों के मद्देनज़र हमारा मानना है कि जाति व्यवस्था को नेस्तनाबूद किये बिना भारत में कोई भी क्रांति और सामाजिक बदलाव की बात करना न सिर्फ एक कोरी कल्पना बल्कि एक गैर-ज़िम्मेदाराना विचार है. जाति व्यवस्था का विनाश ही हमारे समय की सब से बड़ी क्रांति हो सकती है!
साम्प्रदायिकता और जाति प्रश्न
इसके अतिरिक्त, जाति सिर्फ 'हिंदुओं' की बीमारी नहीं बल्कि भारत में सामाजिक स्तरण (social stratification) का मूल तत्व है. जाति अंतर्विरोध हमारे मुल्क का प्रधान अंतर्विरोध है. इस कारण यह यहाँ के सारे समाजों में नज़र आता है. हमारे यहाँ के अल्पसंख्यक समाज भी इसके दायरे के बाहर नहीं हैं. जहाँ मुसलमान 'अशराफ़', 'अजलाफ़' और 'अरजाल' समूहों में बटे हुए हैं, वहीँ सिख समाज 'जाट' और 'मज़हबी' समूहों में और ईसाई 'सिरियन/सारस्वत' और 'दलित ईसाइयों' में विभाजित नज़र आते हैं. ऐसा प्रतीत होता है की हमारे देश के सारे धार्मिक तबके कई जातियों में विभाजित हैं और एक ही समय होता है जब धार्मिक एकता मुमकिन हो पाती है: मज़हबी दंगों के दौरान. आखिर क्या है इन दंगों का राज़? क्या यह महज़ मनोगत कारणों की उपज और स्वतःस्फूर्त परिघटना हैं या कुछ और? कुछ विद्वानों का मानना है कि भारत में धार्मिक दंगे यहाँ के जाति अंतर्विरोध को दबाने कि साज़िश हैं और सारे दबे कुचले तबकों की आवाज़ और जनतांत्रिक मांगों को दरकिनार करने का सबसे प्रबल यंत्र है. अगर गौर से देखा जाये तो धर्म की राजनीति, भले ही वह बहुसंख्यकों की हो या अल्पसंख्यकों की, इन धार्मिक पहचानों में उच्च जातियों / बिरादरियों कि राजनीति है. अगर सरसरी तौर पर भी देखेंगे तो सारे धार्मिक गुरु-नेता और प्रतिष्ठानोँ-इदारों में उच्च जातियों का वर्चस्व पायेंगें. जहाँ हिंदू धार्मिक राजनीति में सवर्णों का नियंत्रण है, वहीँ मुसलमानों में अशराफ तबके का वर्चस्व है. सत्ता की गलियों में भी मुख्यतः सारे धर्मों की उच्च जातियां ही पहुँच पाती हैं.
कई दलित-बहुजन लेखकों ने भारत में 'सेकुलरिस्म' का सिद्धांत और उस ही का जुड़वाँ, मगर दिग्भ्रमित, भाई 'साम्प्रदायिकता' पर आलोचनात्मक रवैया अपनाया है. अगर 'सेकुलरिस्म' के सिद्धांत के इतिहास को देखें तो इस का उद्गम यूरोप में धर्म के भीतर फिरकावाराना (sectarian) झगड़ों से निपटने के लिए हुआ था. भारत में इसको गाँधी के 'सर्व धर्म संभव:' के नज़रिए से परिभाषित किया गया और धर्म के भीतरी द्वंदों के बजाय अंतरधार्मिक झगड़े सुलझाना इसका मुख्य मकसद बना. लिहाज़ा सेकुलरिस्म ने धार्मिक पहचान को भारतियों की प्राथमिक और एकांगी (monolithic) पहचान बनाने का और दूसरी पहचानों को—जैसे जाति, इलाकाई और धार्मिक पंथों/फिरकों—को दरकिनार करने का काम भी किया. लेकिन इस के बीज पहले ही अंग्रेजी उपनिवेशवादी काल में पड़ चुके थे. अगर उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य काल तक भी देखें तो यह नज़र आता है कि यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम ज़मींदार मिलकर किसानों और कमज़ोर जातियों, चाहे वह किसी भी धर्म के हों, के संघर्षों को दबाया करते थे. उस समय कोई आल इंडिया मुस्लिम या हिंदू कौम का तसव्वुर नहीं था बल्कि जाति और पंथ/फिरके ही भारतियों की महत्वपूर्ण पहचानें हुआ करती थीं. लेकिन मुस्लिम और हिंदू अभिजात्य और ज़मींदार वर्ग, या यों कहें कि हिंदू सवर्ण और मुस्लिम अशराफ़ तबकों, की यह एकता १८८० के बाद, जब सांप्रदायिक दंगों का चलन तेज होता है, टूटती हुई नज़र आती है और धीरे-धीरे धार्मिक पहचान यहाँ की मुख्य पहचान बनने लगती है. इस का नतीजा हमें हिंदुस्तान के बँटवारे और उस के साथ जुड़ी मानवीय त्रासदी के रूप में मिलता है. लेकिन यह बात भी गौरतलब है कि हालाँकि बँटवारे के लिए धार्मिक पहचान जिम्मेदार होती है लेकिन आजादी के बाद सेंसस में 'धर्म' का खाना तो जारी रहता है परंतु 'जाति' को निकाल कर बाहर किया जाता है. इस से पहले भी १९३१ के सेंसस में मुस्लिम लीग और राष्ट्रीय स्वयंसेवी संघ 'मुसलमानों' और 'हिंदुओं' को सेंसस में सिर्फ अपनी धार्मिक पहचान दर्ज कराने पर इसरार और गोलबंदी करते हुए नज़र आते हैं. भारत में उच्च जातियों का धार्मिक पहचान की तरफ यह झुकाव दिलचस्प है.
यह साफ़ तौर पर लगता है की सेकुलरिस्म-साम्प्रदायिकता का द्वंद और बहुसंख्यक-अल्पसंख्यक की सियासत एक खास किस्म कि कबड्डी है जिसमे हार खेल में किसी टीम की नहीं बल्कि हमेशा दर्शकों की होती है. इस सियासी खेल में बहुसंख्यक के सवर्ण तबकों के हितों के साथ अल्पसंख्यक तबकों की उच्च जातियों के हित भी सधते हैं, हालाँकि यह भी सही है कि अल्पसंख्यकों के ऊंची बिरादरियों के सियासी कलाकार इस खेल में 'जूनियर पार्टनर' का ही किरदार अदा करते हैं.
'धर्म' और 'धार्मिक पहचान' की राजनीति
मुख्य परिचर्चा को प्रारंभ करने से पहले हम धर्म और धार्मिक पहचान पर आधारित सियासत के बीच फर्क के ऊपर जोर देना चाहते हैं. मज़हब की कई व्याख्याएं मुमकिन हैं. मज़हब एक दार्शनिक और नैतिक व्यवस्था है परंतु यह सनातन और अपरिवर्तनशील नहीं होती. बल्कि धर्म के कैरियर में तमाम उतार-चढ़ाव आते हैं और कई व्याख्याएं और मतभेद उभरते हैं. ताकतवर तबके धर्म की अपनी अवधारणा बनाते हैं और शोषित तबके धर्म की दूसरी व्याख्या करते हैं. इस मायने में धर्म की प्रतिक्रियावादी समझ भी हो सकती है और प्रगतिशील समझ भी. इस संदर्भ में लातिन अमेरिका और साउथ अफ्रीका में ईसाई और इस्लाम धर्म के भीतर से उठे 'लिब्रेशन थेओलोजी' के आंदोलनों ने धर्म का शोषितों के नज़रिए से पुनर्व्याख्या करने का सराहनीय प्रयास किया है. भारत में भी 'दलित लिब्रेशन थेओलोजी' पर विमर्श हो रहा है. इसके बरस्क हम कह चुके हैं कि भारत में धार्मिक पहचान पर होने वाली राजनीति प्रायः उच्च जातियों की राजनीति होती है और सत्ता पर इन जातियों की इजारेदारी पर केंद्रित है. इन उच्च जातियों द्वारा धर्म की की गयी व्याख्या प्रतिक्रियावादी और अंधविश्वासों से भरी है और उसका पूरा जोर जनता को बाँट कर उन पर शासन करना होता है.
यह कहना अनुचित नहीं होगा कि हर तबका अपने हितों, मूल्यों और सामाजिक अवस्थिति (social location) के अनुसार ही अपने धर्म की व्याख्या करेगा या ठुकराएगा और उसी के हिसाब से अपनी 'पहचान की सियासत' का निर्धारण करेगा. भारत का दलित इतिहास और अमरीका में अश्वेतों का इतिहास इस बात का जीता जागता प्रमाण है. यह हम सब जानते हैं कि बाबासाहब अम्बेडकर ने हिंदू धर्म ठुकरा कर बौद्ध धर्म अपनाया था. और बौद्ध धर्म की भी मुख्यधारा अवधारणा की उन्होंने आलोचना की थी तथा 'नवायन' बौद्ध व्याख्या की नींव रखी थी. पहचान के सिलसिले में 'अछूत' से 'हरिजन' से लेकर 'दलित' तक का सफर हम सब जानते हैं. इसी तरह अमरीका में मार्टिन लूथर किंग और माल्कोम एक्स ने भी धर्म की अश्वेतों के नज़रिए से व्याख्या करी. वहाँ पर भी 'नेग्रो' से लेकर 'ब्लैक' तक और फिर 'अफ्रो-अमेरिकेन' तक का सफर दिलचस्प है. कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है की धर्म की व्याख्या और पहचान की सियासत की सामाजिक जड़ें भी होती हैं और आसमानों की सैर कराने वाले मुल्ला-पंडे-पादरी अक्सर मेमने की जगह भेड़ियों के धर्म की बात कर रहे होते हैं.
पसमांदा आंदोलन: धार्मिक एकता या जातीय एकता?
'पसमांदा', जो कि एक फारसी शब्द है, का अर्थ होता है 'वह जो पीछे छूट गया'. कई अर्थों में यह शब्द 'दलित' का समानांतर भी है जिसका मतलब होता है 'दबा-कुचला', 'उत्पीड़ित', 'सताया हुआ', इत्यादि. बिहार में १९९८ में अली अनवर के नेतृत्व में 'आल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज़' के गठन के बाद, जो कि दलित और पिछड़े मुसलमानों का एक सामाजिक संगठन है, यह शब्द काफी लोकप्रिय हुआ. अली अनवर की ही २००१ में लिखित किताब मसावात की जंग ने पसमांदा मुसलमानों की स्थिति के बारे में बहस की और पसमांदा राजनीति की ज़मीन तैयार की. बेशक मुस्लिम समाज में कमज़ोर जातियों के आन्दोलनों का इतिहास पुराना है. आजादी के पहले से 'आल इंडिया मोमिन कांफेरेंस' के हस्तक्षेप, खास तौर पर जिन्नाह के 'दो राष्ट्रों के सिद्धांत' का सीधा विरोध, काबिलेतारीफ हैं. मगर अली अनवर के हस्तक्षेप के बाद इस आन्दोलन ने एक गुणात्मक छलांग लगाई है इस पर दो राय नहीं हो सकती हैं.
जैसा कि हम ज़िक्र कर चुके हैं भारत की मुसलमान आबादी मुख्यतः तीन श्रेणियों में बाटी जा सकती है: अशराफ़, अजलाफ औए अर्ज़ाल. अशराफ़ श्रेणी में मुसलमानों कि उच्च बिरादरियां—जैसे कि सय्यद, शैख़, मुग़ल, पठान और मल्लिक—आते हैं. अजलाफ़ श्रेणी में शूद्र तबके से धर्म परिवर्तित कर के आयी जातियां—तेली, जुलाहे, राईन, धुनिये इत्यादि—शामिल की जा सकती हैं. इसी तरह अर्ज़ाल श्रेणी में दलित या अतिशूद्र जातियों से जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया—जैसे कि हलालखोर, बक्खो, कसाई, इत्यादि—को शामिल किया जा सकता है. अगर जनसंख्या के हिसाब से देखें तो अजलाफ़ और अर्ज़ाल तबके मिलकर भारतीय मुसलमानों की कुल आबादी का कम-से-कम ८५% होते हैं. अजलाफ़ तबके को मुसलमानों का शूद्र या पिछड़ा वर्ग कहा जा सकता है और अर्ज़ाल तबके को मुसलमानों का दलित या अनुसूचित जाति में रखा जा सकता है. पसमांदा आंदोलन, बहुजन आन्दोलन की तरह, मुसलमानों के पिछड़े और दलित तबकों की नुमांयदगी करता है और उनके मुद्दों को उठाता है. यह भारत की मुख्यधारा की मुसलमानों की सियासत को 'अशराफिया राजनीति' मानता है और उसे चुनौती देता है.
आखिर क्या है अशराफिया राजनीति? यह मुसलमानों के अभिजात्य उच्च-जातियों की राजनीति है जो कि सिर्फ कुछ सांकेतिक और जज़्बाती मुद्दों को—जैसे कि बाबरी मस्जिद, उर्दू, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, पर्सनल लॉ, इत्यादि—को उठाती रही है. इन मुद्दों पर गोलबंदी कर के और मुसलमानों की भीड़ दिखा के मुसलमानों के अशराफ़ तबके और उनके संगठन—जमीअत-ऐ-उलेमा-ऐ-हिंद, जमात-ऐ-इस्लामी, आल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड, मुस्लिम मजलिस-ऐ-मशावारात, पोपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इत्यादि—अपना हित साधते रहे हैं और सरकार में अपनी जगह पक्की करते हैं. इनका पूरा तर्ज़े-अमल अजनतान्त्रिक है और इस तरह के जज्बाती मुद्दों के ज़रिये यह अपना प्रतिनिधित्व तो कर लेते हैं मगर पसमांदा मुसलमानों की बलि चढ़ा कर. जाहिरा तौर पर यह कुछ पसमांदा तबके के व्यक्तियों को, जिनका 'अशराफिकरण' हो चुका है, आगे तो रखते हैं लेकिन किसी नेकनियती के तहत नहीं बल्कि मुस्लिम समाज के जाति तजाद को नियंत्रित करने के लिए. दिलचस्प बात है कि इन ही मुद्दों पर—बाबरी मस्जिद, उर्दू, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, पर्सनल लॉ—तमाम हिंदू संघटनों, जैसे कि आर. एस. एस., विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, वगैरह, की भी राजनीति फलती-फूलती है. आखिरकार ताली दोनों हाथों से ही तो बजती है!
ज़ाहिर है कि इस जज़्बाती राजनीति में पसमांदा आबादी, जो कि ज़्यादातर कारीगर-दस्तकार हैं और मेहनत-मजदूरी कर के अपना जीवनयापन करती है, के मुद्दे और परेशानियों के लिए जगह कहाँ हो सकती है. मुख्यधारा की मुस्लिम संस्कृति में क़व्वाली, ग़ज़ल, दास्तानगोई, कुरान के ऊपर अक्ली व्यायाम का तो शुमार होगा लेकिन बक्खो के गीत, जुलाहों का करघा, मीरशिकार के किस्सों का ज़िक्र कैसे हो सकता है. मुस्लिम लीडरान और प्रसिद्ध व्यक्तियों में अशराफ़ तबके के अबुल कलाम आज़ाद , सर सैय्यद अहमद खान, मुहम्मद अली जिन्नाह, अल्लामा इकबाल, वगैरह का ज़िक्र तो होना ही है मगर पसमांदा तबके के अब्दुल कैयूम अंसारी, वीर अब्दुल हमीद, मौलाना अतीकुर्रहमान आरवी, आसिम बिहारी का ज़िक्र कहाँ. और जब दंगों में बस्तियां जलती हैं तो उस में भी अकसरियत पसमांदा मुसलमानों की ही होती है. चोट किसी को लगे और मरहम किसी और को!
कुछ आंकड़े दे कर बात बढ़ाते हैं. अगर पहली से लेकर चौदहवीं लोक सभा की लिस्ट उठा कर देखें तो पाएंगे कि तब तक चुने गए सभी ७५०० प्रतिनिधियों में ४०० मुसलमान थे. और इन ४०० मुसलमान प्रतिनिधियों में केवल ६० पसमांदा तबके से थे. अगर भारत में मुसलमानों की आबादी कुल आबादी की १३.४ % (२००१ सेंसस) है तो अशरफिया आबादी २.१ % (जो कि मुसलमान आबादी के १५ % हैं) के आसपास होगी. हालांकि, लोक सभा में उनका प्रतिनिधित्व ४.५ % है जो कि उनकी आबादी से कहीं ज्यादा है. साफ़ ज़ाहिर है कि मुस्लिम/अल्पसंख्यक सियासत से किस तबके को लाभ मिल रहा है और सचर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमीशन की सारी मुस्लिम कौम को पिछड़ा दिखाने की कोशिश और सारे मुसलमानों को आरक्षण के दायरे में लाने पर बहसें क्यों पसमांदा आन्दोलन के गले से नीचे नहीं उतरती है. हम इस ही निष्कर्ष में पहुँच सकते हैं कि जिस तरह 'हिंदू' राजनीति से दलित-बहुजन को कोई फायदा नहीं है, उस ही तरह 'मुस्लिम' राजनीति से पसमांदा का भी कोई लाभ नहीं होने वाला है. यह दोनों राजनीतियां सभी धर्मों की कमज़ोर जातियों को आपस में लड़ा कर उच्च जातियों के हित सुरक्षित करने का काम ही करती हैं. इस लिए 'धार्मिक पहचान की राजनीति' का अब तिरस्कार करना पड़ेगा और धर्म के आधार पर एकता को कमज़ोर कर के सभी धर्मो की कमज़ोर जातियों की एकता पर ध्यान देना होगा. ज़ाहिर सी बात है कि इस से 'इस्लाम खतरे में है' और 'गर्व से कहो हम हिंदू हैं' का नारा उठेगा. देश की पसमांदा-बहुजन आबादी को अब समझ लेना चाहिए कि जिस 'इस्लाम' और 'हिंदू' धर्म की ओर यह नारे इशारा कर रहे हैं वह उनके नहीं. उन के इस्लाम और हिंदू धर्म की कुछ पुनर्व्याख्या हुयी है और काफी अभी होनी बाक़ी है. वक्त के साथ जब यह तबके कलम पकड़ेंगे तो वह भी होगा.
जब मुसलमानों में जाति का सवाल उठता है तो कई मुस्लिम विद्वान छटपटाहट के साथ कहते हैं कुरान में जात-पात कहाँ. पर यहाँ सवाल कुरान का नहीं उस की व्याख्या का है. और किसी भी किताब कि व्याख्या व्यक्तिपरक (subjective) होती है और लेखक की सामाजिक अवस्थिति पर भी निर्भर करती है. जब मौलाना अशराफ अली थानवी बहिश्ती ज़ेवर में 'कुफु' के सिद्धान्त को बयान करते हुए यह बताते हैं कि ऊंची बिरादरियों को नीची बिरादरियों के साथ विवाह के संबंध नहीं कायम करने चाहिए तो मौलाना और उनके मुरीदों को यह इस्लामी सिद्धांत ही लग रहा था. कुरान में मसावात और बराबरी के नियम का बयान करने वाले उलेमा को इस बात का भी ज़िक्र करना चाहिए कि मुस्लिम मुल्कों में गुलामी प्रथा का खात्मा १५०० साल के इस्लाम के अस्तित्व के बाद भी पिछली सदी में ही क्यों मुमकिन हुआ. हर व्यावहारिक मसले के लिए हमारा पाला कुरान से नहीं उसकी व्याख्या से पड़ता है. और अब तक यह बात साफ़ हो चुकी होगी कि कुरान कि व्याख्या भारत में कौन सा तबका करता है. बुनियादी तौर पर धर्म-ग्रंथों की व्याख्या का मामला भी राजनीतिक और सामाजिक होता है. इस लिए प्रभावशाली तबकों द्वारा किये गए व्याख्याओं का जवाब भी राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन के आन्दोलनों के साथ ही दिया जायेगा.
इस के अतिरिक्त जिन लोगों को लगता है कि मुसलमानों में जाति व्यवस्था हिंदुओं के मुकाबले कमज़ोर है तो उनको यह ध्यान रखना चाहिए कि जाति व्यवस्था बुनियादी तौर पर 'सामाजिक बहिष्करण' (social exclusion) के लिए अस्तित्व में आई है. इस का रूप अवश्य क्षेत्रीय और धार्मिक तौर पर भिन्न हो सकता है परन्तु इस कि मार नहीं. आखिर कितने इलाके हैं भारत में जहाँ मनु स्मृति में वर्णित जाति व्यवस्था हूबहू मिलती है? क्या दक्षिण भारत में उपलब्ध होने वाली व्यवस्था उत्तर भारत से भिन्न नहीं? क्या पश्चिमी बंगाल और उत्तर प्रदेश में यह समान रूप से काम करती है? इस लिए ज़रूरी सवाल यह है की यह निजाम किस तरह से, किन और कितने तबकों को और कितने प्रभावशाली तरीके से सत्ता, ज्ञान और अर्थ के दायरे से बाहर रखता है. जहाँ तक रूप (form) का सवाल है तो यह मुसलमानों में रोटी-बेटी के रिश्तों में, विभिन्न जातियों के अलग कब्रिस्तान होना, कुछ मस्जिदों में नमाज़ के दौरान कमज़ोर जातियों को पीछे की सफों में ही खड़े होने की इजाज़त देना, दलित मुसलमान तबकों के साथ कुछ इलाकों में छुआछूत का प्रचलन, अशरफिया जातियों का कुछ इलाकों में कमज़ोर जातियों की मस्जिदों का जलाना, इत्यादि, में नज़र आता है. जहाँ तक धार्मिक वैधता का प्रश्न है मसूद फलाही की किताब हिन्दुस्तान में ज़ात-पात और मुसलमान यहाँ के उलेमा और मौलवियों के जातिवादी चरित्र को साफ़ तौर पर नुमाया करती है.
तीन मुख्य सवाल: बहुलतावाद, लोकतंत्र, विकास
इस संदर्भ में पसमांदा राजनीति को तीन मुख्य सवालों पर ध्यान केंद्रित करना होगा: बहुलतावाद, जनतंत्र और विकास. ध्यान रहे कि यह तीनों सवाल भारतीय राजनीति के एजेंडा में १९९० के दशक में बाबरी मस्जिद के विध्वंस, मंडल कमीशन की एक अनुशंसा (केंद्रीय नौकरियों में ओबीसी को आरक्षण) का लागू होना और आर्थिक सुधारों की शुरुआत के साथ बने हुए हैं.
सब से पहले बहुलतावाद (pluralism) पर चर्चा करते हैं. हम कह चुके हैं की सांप्रदायिक दंगे भारत में दबे कुचले तबकों और शोषित जातियों की जनतांत्रिक मांगों को दबाने का एक हथियार है. इस ही लिए बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि का विवाद मंडल क्रांति को दबाने के लिये खड़ा किया गया. याद रहे कि मंडल सिफारिशों नें ८० के करीब पसमांदा मुस्लिम जातियों को ओबीसी श्रेणी में रख कर मुसलमानों में अशराफ तबकों की उतनी ही नींद उड़ाई थी जितनी हिंदुओं में सवर्ण तबकों की. इस के अलावा अब इतिहास से ठोस प्रमाण मिल रहे हैं कि यह उपाय कोई नया नहीं. कुछ इतिहासकारों नें साफ़ तौर पर कहा है कि कम से कम १८८० के बाद से भारत में हर सांप्रदायिक दंगा किसी न किसी कमजोर वर्गों में जातीय उभार या आंदोलन को कुचलने के लिए हुआ है. साफ़ है कि सांप्रदायिक दंगों का सफाया 'अंतरधार्मिक संवाद' और 'शांति मार्च' से नहीं होगा क्योंकि इनका कारण मनोगत (subjective) नहीं बल्कि संग्रच्नात्मक (structural) है. इस का हल सिर्फ जाति व्यवस्था के विध्वंस के साथ ही हो सकता है. इस लिए भारत में बहुलतावाद का प्रश्न जाति के प्रश्न के साथ सीधा सम्बन्ध रखता है. इस लिए यहाँ पर धर्म की एकता को छोड़ कर अब जातीय एकता कि बात करनी चाहिए. 'दलित-पिछड़ा एक सामान, हिंदू हो या मुसलमान' का नारा ही अब यहाँ पर साम्प्रदायिकता के जिन्न को बंद कर सकता है. इस नारे को ज़मीनी हकीकत बनाने के लिए पसमांदा आंदोलन को भरसक प्रयास करना पड़ेगा.
दूसरा अहम सवाल लोकतंत्र को गहरा करने का है. इस संदर्भ में मंडल ने सराहनीय हस्तक्षेप किया था. हालाँकि इस सवाल के दो सम्बंधित पहलू हैं: १) सत्ता का जनतंत्रीकरण होना और, २) इस दिशा में संघर्ष करने वाले संगठन और पार्टियों के आंतरिक जनतंत्र का प्रश्न. जैसा कि अम्बेडकर ने बताया था भारत में 'क्रमिक असमानता' है और यहाँ पर हर जाति अपने से नीचे जातियों को कमतर समझती है और अपने ऊपर वाली जातियों के सामने सर झुकाती है. इस का प्रभाव रोटी-बेटी के रिश्तों पर साफ़ दीखता है. इस लिए पिछड़ी और दलित जातियां भी बटी हुई हैं और अक्सर उनके नेता अपनी मूल जाति के हितों से बाहर नहीं निकल पाते. जहाँ लालू यादव और मुलायम सिंह यादव पर यह इलज़ाम लगता है कि उनकी पार्टियां 'अहीरों' की पार्टियां बन गयीं थीं, वहीँ मायावती पर 'जाटवों' और रामविलास पासवान को 'दुसाधों' पर अत्यधिक ध्यान देने का इल्ज़ाम लगता है. पसमांदा संगठनों की भी यह समस्या है. अली अनवर के संघटन का जोर 'जुलाहों' पर ज्यादा है तो डॉ एजाज़ अली का ध्यान 'राईनों' पर. पसमांदा राजनीति को सामाजिक न्याय के बुनियादी सिद्धांत 'जिसकी जितनी आबादी, उस की उतनी हिस्सेदारी' को गंभीरता से लेना होगा और अपने संगठनों और पार्टियों पर इसे लागू करना होगा. पार्टी के हर स्तर पर कमेटियों में हर बिरादरी का उसकी आबादी के अनुसार प्रतिनिधित्व होना चाहिए. इस के अलावा 'एक लीडर, एक पार्टी' के सिद्धांत के ऊपर पुनः सोचने कि ज़रूरत है. भारत जैसे समाज में नायकों और महात्माओं की भक्ति का रिवाज गहरी जड़ें जमा चुका है और इस को चुनौती देने कि ज़रूरत है. किसी भी व्यक्ति विशेष पर निर्णय लेने की ज़िम्मेदारी केंद्रित करने कि जगह पर आज़ादाना बहस-मुबाहिसे के ज़रिये फैसले लेने कि प्रणाली पर काम करना होगा. जहाँ पर मतैक्य मुमकिन नहीं वहाँ पर 'एक व्यक्ति, एक वोट' के सिद्धांत के तहत फैसले लेने चाहिए. केंद्र में व्यक्ति नहीं बल्कि राजनीति और विचारधारा होनी चाहिए. सवाल एक लीडर का नहीं है बल्कि पूरे पसमांदा समाज में अनेक लोगों को नेतृत्व सँभालने के लिए तैयार करने का है. इस लिए 'प्रक्रिया' पर जोर होना चाहिए न कि किसी व्यक्ति विशेष पर. एक और अहम सवाल जनतंत्र के पहिये को पूरा घुमाने का है और यह सुनिश्चित करने का कि हर तबके को सत्ता में भागीदारी मिले. इस सन्दर्भ में 'अति-पिछड़ा वर्ग' और 'महादलित' श्रेणी पर बहस करने कि ज़रूरत है और इस सन्दर्भ में कुछ आगे बढ़ चुके पिछड़े और दलित समूहों को दरियादिली दिखानी होगी. उन से कोई क़ुरबानी की मांग नहीं कर रहा है, सिर्फ सामाजिक न्याय के नियमों के तहत इन्साफ की उम्मीद है. इसके अतिरिक्त अब 'निर्वाचकीय निज़ाम' पर भी बात करने की ज़रूरत है. भारत में अभी रायज 'फर्स्ट-पास्ट-दी-पोस्ट सिस्टम' में वह पार्टी जो सब से अधिक सीट लाती है सरकार बनाती है. ऐसे में यह मुमकिन है की जिसको २५% वोट मिले हों उसे १५० सीटें मिल जाए और जिसे २२ % वोट मिले हों उसे केवल ३० ही सीट मिलें. इस तरह के नतीजे जनादेश की सही नुमाइंदगी नहीं करते. भारत में कुछ संगठन अब 'प्रोपोर्शनल इलेक्टोरल सिस्टम्' की वकालत कर रहे हैं जहाँ पर किसी भी पार्टी की सीटों की तादाद वोट-शेयर पर निर्भर करेगी. यह ज़्यादा मुंसिफाना निज़ाम है और इस को एजेंडा में शामिल करने कि ज़रूरत है. [अधिक जानकारी के लिए देखें: http://www.ceri.in/]. एक बड़ा मसला यह भी है की भारत में सरकारी कर्मचारियों का राजनीति में हिस्सा लेना या राजनीतिक मुद्दों पर लिखने की इजाज़त नहीं है. इस से पसमांदा-बहुजन समाज का एक बड़ा बुद्धिजीवी तबका राजनीति में सक्रिय भागीदारी नहीं कर पाता है. यह नागरिकता के अधिकारों का उल्लंघन है और इस पर अब खुल कर चर्चा करनी चाहिए.
आखिरी सवाल विकास के मॉडल का है. आर्थिक सुधारों ने भारत में काफी दूरगामी परिवर्तन किये हैं. एक तरफ तो बड़ी राष्ट्रीय एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों का वर्चस्व बढ़ा है और मध्यम वर्ग का फैलाव हुआ है, वहीँ दूसरी ओर कई लघु उद्योग, कारीगरों और दस्तकारों पर काफी नकारात्मक असर भी पड़ा है. अभी तक पसमांदा राजनीति ने सरकार से बुनकरों के क़र्ज़ माफ करने, इत्यादि की मांगें रखीं हैं. परंतु यह मांगें अगर मान भी ली गईं तो अस्थाई राहत ही देंगीं. भूमंडलीकरण के इस युग में, जहाँ पर सूचना और यातायात क्रांति हो रही है, उत्पादन प्रणाली और बाज़ार में आमूलचूल परिवर्तन हो रहे हैं. इसका असर लगभग सारे कारोबारों पर पड़ रहा है. पसमांदा तबके में एक बड़ी आबादी पुश्तैनी पेशों से जुड़ी हुई है (अभी तक सिर्फ बुनकरों पर जोर रहा है). इन सारे कारोबारों पर शोध करने कि ज़रूरत है और उस ही हिसाब से हस्तक्षेप करना होगा. कुछ कारोबारों में सस्ते दरों में ऋण/लोन उपलब्ध कराने से काम चलेगा, कुछ में पुनर्प्रशिक्षण की ज़रूरत होगी, कुछ में नई तकनीक प्रचलित करनी होगी, इत्यादि. इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा की स्कीमों, कार्यस्थल में जम्हूरियत, कॉर्पोरेट डाईवर्सिटी, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी, निजि छेत्र में आरक्षण, गवर्नेंस, वगैरह, जैसे मुद्दों पर भी बहस करने की ज़रूरत है.
बिहार में हालिया विधान सभा चुनाव परिणामों के बाद से मीडिया लगातार इस बात का प्रचार कर रही है कि बिहार का चुनाव परिणाम विकास की जीत तथा जाति की राजनीति (अर्थात सामाजिक न्याय) की हार है. विकास और सामाजिक न्याय को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है मानो सामाजिक न्याय का विकास से से कोई बुनियादी अंतर्विरोध हो. पसमांदा समेत समूचे सामाजिक न्याय के आंदोलन को पूंजीवादी और अभिजात मीडिया द्वारा प्रचारित, प्रसारित और पोषित विकास के चालू मॉडल को रिजेक्ट करने की घोषणा करनी चाहिए क्यों कि विकास के मौजूदा मॉडल में न केवल बहुजन कहीं नहीं हैं बल्कि यह बहुजनों के खिलाफ चलाया जा रहा है. सेंसेक्स के उठाव और गिराव को विकास का पैमाना मानन
--
Palash Biswas
Pl Read:
http://nandigramunited-banga.blogspot.com/







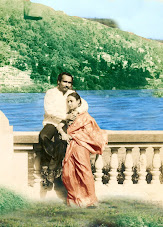












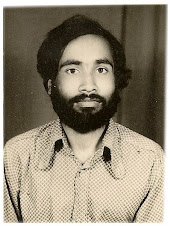

No comments:
Post a Comment